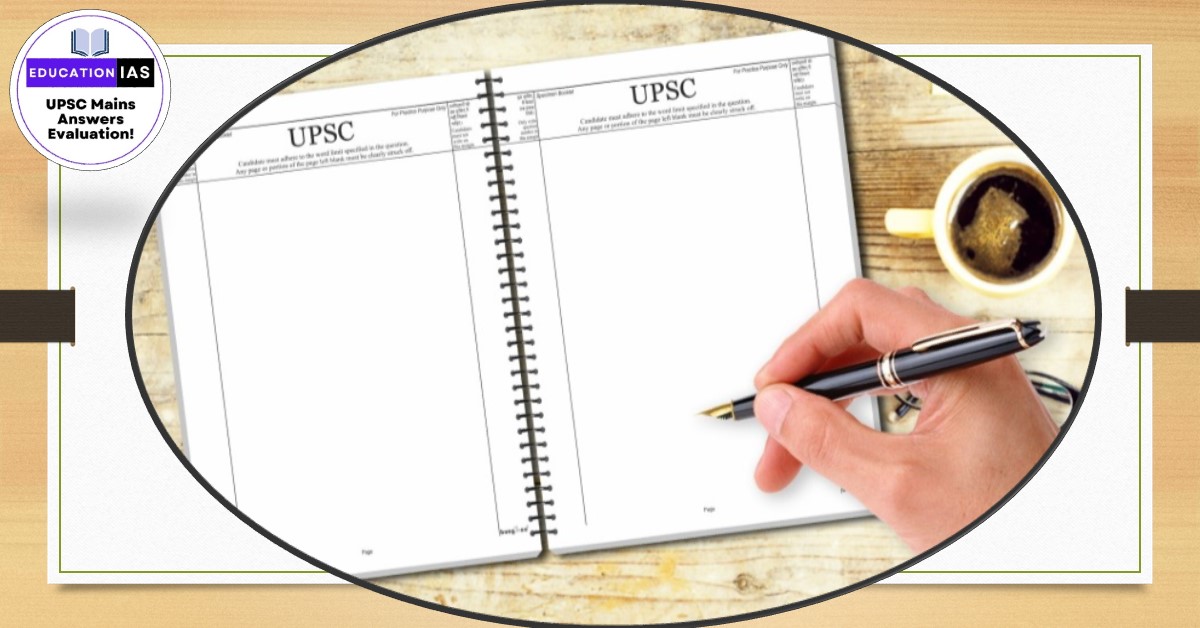प्रश्न: भारत में भूस्खलन के कारणों का परीक्षण कीजिए, जिसमें प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये कारक किस प्रकार भिन्न हैं?
Examine the causes of landslides in India, focusing on both natural and anthropogenic factors. How do these factors vary across different regions of the country?
उत्तर: भूस्खलन एक भूगर्भीय प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी, चट्टानों और मलबे का अस्थिर होकर ढलान पर नीचे गिरना शामिल होता है। यह प्राकृतिक तथा मानवजनित कारकों के परिणामस्वरूप होता है। भारत में भूस्खलन विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है, जिससे जीवन, अधोसंरचना और पारिस्थितिकी प्रभावित होती है।
भारत में भूस्खलन के प्राकृतिक कारण
(1) भू-आकृतिक संरचना: भारत में विशेष रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट क्षेत्रों की भू-आकृतिक संरचना अस्थिर है। इन क्षेत्रों का निर्माण हाल ही में हुआ है, जिससे इनकी मिट्टी और चट्टानें पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं हैं। इसी कारणवश भूस्खलन की घटनाएं यहां अधिक होती हैं, जिससे मानव बस्तियां और बुनियादी ढांचा प्रभावित होते हैं।
(2) भारी वर्षा और जलभराव: भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। जलभराव मिट्टी की स्थिरता को प्रभावित करता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना बढ़ती है। मानसून के दौरान पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में भूस्खलन अधिक होते हैं, जिससे लोगों के जीवन और आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
(3) भूकंप और ज्वालामुखीय हलचल: भारत का हिमालयी क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप के कारण भूमि की सतह अस्थिर होती है और इससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। कुछ क्षेत्रों में ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण भी जमीन की सतह कमजोर होती है। ये घटनाएं पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ाती हैं और स्थानीय समुदायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
(4) पर्वतीय जलधारा का कटाव: नदियों और जलधाराओं द्वारा पहाड़ियों की सतह का लगातार कटाव होता रहता है, जिससे उनकी मिट्टी कमजोर हो जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जलधारा के कारण भूमि अस्थिर हो जाती है। इससे स्थानीय निवासियों की सुरक्षा प्रभावित होती है और कृषि एवं संरचनात्मक विकास को नुकसान पहुंचता है।
(5) जलवायु परिवर्तन: बदलते मौसम और तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ रही है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिरता प्रभावित होती है और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं। अनियमित वर्षा, बढ़ती गर्मी और अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन से भूस्खलन की तीव्रता अधिक हो जाती है, जो दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय चुनौतियां उत्पन्न करता है।
भारत में भूस्खलन के मानवजनित कारण
(1) अनियंत्रित निर्माण कार्य: बिना उचित भूगर्भीय अध्ययन के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों, भवनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया जाता है। इससे प्राकृतिक भू-आकृति प्रभावित होती है, और भूमि की स्थिरता कमजोर पड़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं, जो स्थानीय निवासियों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
(2) वनों की कटाई: वनस्पति मिट्टी को स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन अत्यधिक वनों की कटाई से भूमि की पकड़ कमजोर हो जाती है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का अपरदन बढ़ता है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में इस कारणवश भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
(3) खनन गतिविधियां: खनिज और पत्थर उत्खनन के दौरान विस्फोटकों के उपयोग से भूमि की सतह कमजोर हो जाती है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय जैसे खनन क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण पर्यावरणीय अस्थिरता उत्पन्न हो रही है।
(4) जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन: अत्यधिक जल निकासी और भूजल के अनियंत्रित दोहन से मिट्टी की संरचना कमजोर होती है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिरता प्रभावित होती है और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं। पश्चिमी घाट और अरावली क्षेत्र इस समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जिससे जलवायु संतुलन बिगड़ रहा है।
(5) अव्यवस्थित कृषि पद्धतियां: अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और असंगठित कृषि प्रणाली के कारण भूमि की गुणवत्ता कमजोर होती है। इससे मिट्टी का अपरदन बढ़ता है और भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की स्थिरता बनाए रखने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है।
भारत में भूस्खलन के क्षेत्रीय कारक
(1) हिमालयी क्षेत्र (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर): हिमालयी राज्यों में तीव्र ढलान और अस्थिर चट्टानों के कारण भूस्खलन की घटनाएँ आम हैं। भूकंप से भूमि अस्थिर होती है, जिससे मिट्टी और चट्टानें गिरती हैं। अनियंत्रित निर्माण कार्य और वनों की कटाई से मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है, जिससे जोखिम बढ़ता है।
(2) पश्चिमी घाट (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु): पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारी मानसूनी वर्षा और अत्यधिक जलभराव के कारण भूस्खलन होता है। पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी की पकड़ कमजोर होने से ये घटनाएँ अधिक देखी जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा तीव्र हुई है, जिससे इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी है।
(3) पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम): पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना अपेक्षाकृत कमजोर है, जिससे यहाँ भूस्खलन की घटनाएँ अधिक होती हैं। इस क्षेत्र में वनों की कटाई और अनियमित मौसम परिवर्तन के कारण भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ी हैं। खनन गतिविधियों से चट्टानों की स्थिरता प्रभावित होती है, जिससे वर्षा के दौरान मिट्टी खिसकती है।
(4) दक्षिण भारत (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल): दक्षिण भारत में भूस्खलन की घटनाएँ मुख्य रूप से जल निकासी की अव्यवस्था और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की पकड़ कमज़ोर होने से भूमि अस्थिर होती है। खनन और निर्माण कार्य से भूगर्भीय संतुलन प्रभावित होता है, जिससे जोखिम बढ़ता है।
(5) अरावली और विंध्याचल क्षेत्र (राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़): अरावली और विंध्याचल क्षेत्र में भूस्खलन मुख्य रूप से खनन, जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण होता है। अनियंत्रित भूमि दोहन से मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है। वर्षा के दौरान भू-स्खलन की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है।
भारत में भूस्खलन प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारणों से उत्पन्न होता है। यह केवल पर्यावरणीय असंतुलन नहीं उत्पन्न करता, बल्कि मानव जीवन और आधारभूत संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक भू-प्रबंधन, पुनर्वनीकरण, सतत विकास रणनीतियाँ और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।